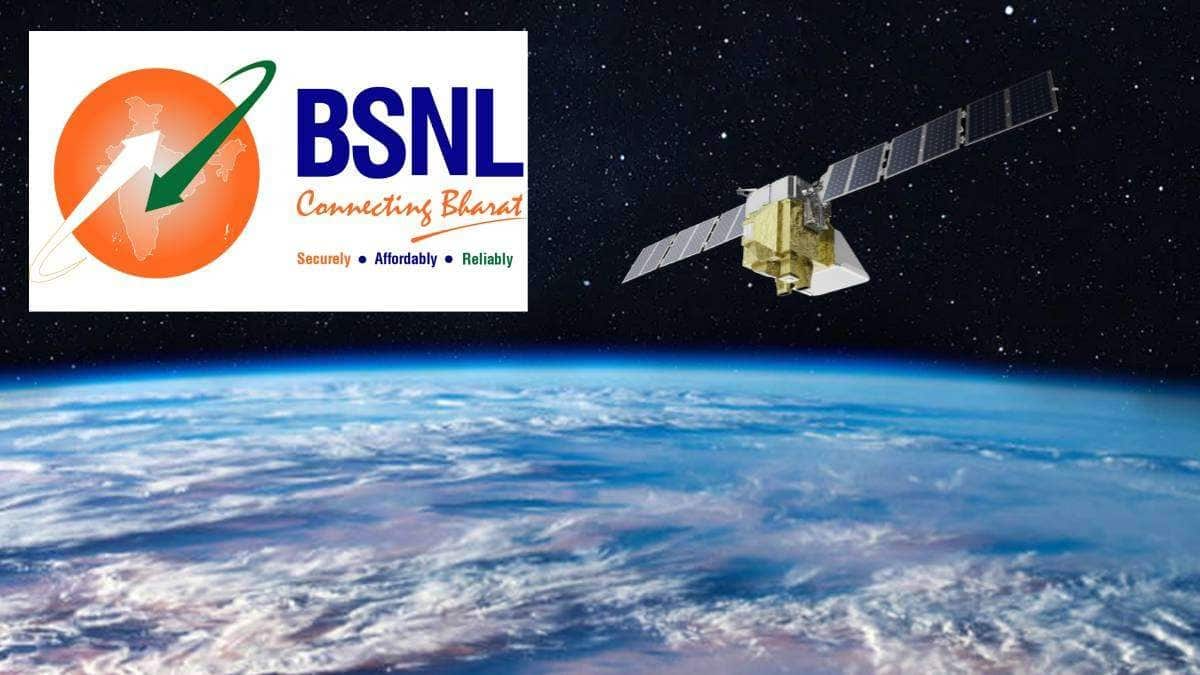हम किसी और के संसार में रहने लगे हैं…. गांधी विचारक धर्मपाल
धर्मपाल जी विख्यात चिंतक एवं गांधी विचारक हैं। प्रस्तुत है उनका लिखा एक आलेख…
भारतीय मानस में सृष्टि के विकास के क्रम और उसमें मानवीय प्रयत्न और मानवीय ज्ञान-विज्ञान के स्थान की जो छवि अंकित है, वह आधुनिकता से इस प्रकार विपरीत है तो इस विषय पर गहन चिंतन करना पड़ेगा। यहां के तंत्र हम बनाना चाहते हैं और जिस विकास प्रक्रिया को यहां आरंभ करना चाहते हैं, वह तो तभी यहां जड़ पकड़ पाएगी और उसमें जनसाधारण की भागीदारी तो तभी हो पायेगी जब वह तंत्र और विकास प्रक्रिया भारतीय मानस और काल दृष्टि के अनुकूल होगी। इसलिए इस बात पर भी विचार करना पडे़गा कि व्यवहार में भारतीय मानस पर छाए विचारों और काल की भारतीय समझ के क्या अर्थ निकलते है? किस प्रकार के व्यवहार और व्यवस्थाएं उस मानस व काल में सही जँचते हैं? सम्भवत: ऐसा माना जाता है कि मानवीय जीवन और मानवीय ज्ञान की क्षुद्रता का जो भाव भारतीय सृष्टि-गाथा में स्पष्ट झलकता है, वह केवल अकर्मण्यता को ही जन्म दे सकता है पर यह तो बहुत सही बात है। किसी भी विश्व व काल दृष्टि का व्यवाहारिक पक्ष तो समय सापेक्ष होता है। अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग समय पर उस दृष्टि की अलग-अलग व्याख्याएं होती जाती हैं। इन व्याख्याओं से मूल चेतना नहीं बदलती पर व्यवहार और व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं और एक ही सभ्यता कभी अकर्मण्यता की और कभी गहन कर्मठता की ओर अग्रसर दिखाई देती है।
भारतीय परंपरा में किसी समय विधा और ज्ञान का दो धाराओं में विभाजन हुआ है। जो विधा इस नश्वर सतत परिवर्तनशील, लीलामयी सृष्टि से परे के सनातन ब्रह्म की बात करती है। उस ब्रह्म से साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है वह परा विधा है। इसके विपरीत जो विधाएं इस सृष्टि के भीतर रहते हुए दैनंदिन की समस्याओं के समाधान का मार्ग बतलाती हैं। साधारण जीवन-यापन को संभव बनाती हैं। वे अपरा विधाएं है। और ऐसा माना जाता है कि परा विधा, अपरा विधाओं से ऊँची है।
अपरा के प्रति हेयता का भाव शायद भारतीय चित्त का मौलिक भाव नहीं है। मूल बात शायद अपरा की हीनता की नहीं थी। कहा शायद यह गया था कि अपरा में रमते हुए यह भूल नहीं जाना चाहिए कि इस नश्वर सृष्टि से परे सनातन सत्य भी कुछ है। इस सृष्टि में दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य करते हुए परा के बारे में चेतन रहना चाहिए। अपरा का सर्वदा परा के आलोक में नियमन करते रहना चाहिए। अपरा विधा की विभिन्न मूल संहिताओं में कुछ ऐसा ही भाव छाया मिलता है। पर समय पाकर परा से अपरा के नियमन की यह बात अपरा की हेयता में बदल गई है। यह बदलाव कैसे हुआ इस पर तो विचार करना पडे़गा। भारतीय मानस व काल के अनुरूप परा और अपरा में सही संबंध क्या बैठता है, इसकी भी कुछ व्याख्या हमें करनी ही पड़ेगी।
पर यह ऊँच-नीच वाली बात तो बहुत मौलिक नहीं दिखती। पुराणों में इस बारे में चर्चा है। एक जगह ऋषि भारद्वाज कहते है कि यह ऊँच-नीच वाली बात कहां से आ गई? मनुष्य तो सब एक ही लगते है, वे अलग-अलग कैसे हो गए? महात्मा गाँधी भी यही कहा करते थे कि वर्णो में किसी को ऊँचा और किसी को नीचा मानना तो सही नहीं दिखता। 1920 के आस-पास उन्होंने इस विषय पर बहुत लिखा और कहा। पर इस विषय में हमारे विचारों का असंतुलन जा नहीं पाया। पिछले हजार दो हजार वर्षों में भी इस प्रश्न पर बहस रही होगी। लेकिन स्वस्थ वास्तविक जीवन में तो ऐसा असंतुलन चल नहीं पाता। वास्तविक जीवन के स्तर पर परा व अपरा के बीच की दूरी और ब्राह्मण व शूद्र के बीच की असमानता की बात भी कभी बहुत चल नहीं पाई होगी। मौलिक साहित्य के स्तर पर भी इतना असंतुलन शायद कभी न रहा हो। यह समस्या तो मुख्यत: समय-समय पर होने वाली व्याख्याओं की ही दिखाई देती है।
पुरूष सूक्त में यह अवश्य कहा गया है कि ब्रह्म के पांवों से शूद्र उत्पन्न हुए, उसकी जंघाओं से वैश्य आए, भुजाओं से क्षत्रिय आए और सिर से ब्राह्मण आए। इस सूक्त में ब्रãह्म और सृष्टि में एकरूपता की बात तो है। थोड़े में बात कहने का जो वैदिक ढंग है उससे यहाँ बता दिया गया है कि यह सृष्टि ब्रह्म का ही व्यास है, उसी की लीला है। सृष्टि में अनिवार्य विभिन्न कार्यो की बात भी इसमें आ गई है। पर इस सूक्त में यह तो कहीं नहीं आया कि शूद्र नीचे है और ब्राह्मण ऊँचे है। सिर का काम पांवों के काम से ऊँचा होता है। यह तो बाद की व्याख्या लगती है। यह व्याख्या तो उलट भी सकती है। पांवों पर ही तो पुरूष धरती पर खडा़ होता है। पांव टिकते हैं तो ऊपर धड़ भी आता है हाथ भी आते हैं। पांव ही नहीं टिकेंगें तो और भी कुछ नहीं आएगा। पुरूष सूक्त में यह भी नहीं है कि ये चारों वर्ण एक ही समय पर बने। पुराणों की व्याख्या से तो ऐसा लगता है कि आरंभ में सब एक ही वर्ण थे। बाद में काल के अनुसार जैसे-जैसे विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की आवष्यकता होती गई, वैसे-वैसे वर्ण-विभाजित होते गए।
कर्म और कर्मफल के इस मौलिक सिद्धांत का इस विचार से तो कोई संबंध नहीं है कि कुछ कर्म अपने आप में निकृष्ट होता है और कुछ प्रकार के काम उत्तम। वेदों का उच्चारण करना ऊँचा काम होता है और कपडा़ बुनना नीचा काम, यह बात तो परा-अपरा वाले असंतुलन से ही निकल आई है। और इस बात की अपने यहाँ इतनी यांत्रिक-सी व्याख्या होने लगी है कि बड़े-बड़े विद्वान भी दरिद्रता, भुखमरी आदि जैसी सामाजिक अव्यवस्थाओं को कर्मफल के नाम पर डाल देते हैं। श्री ब्रह्मा नंद सरस्वती जैसे जोशीमठ के ऊँचे शंकराचार्य तक कह दिया करते थे कि दरिद्रता तो कर्मो की बात है। करूणा, दया, न्याय आदि जैसे भावों को भूल जाना तो कर्मफल के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं हो सकता। यह तो सही व्याख्या नहीं दिखती।
कर्मफल के सिद्धांत का अर्थ तो शायद कुछ और ही है। क्योंकि कर्म तो सब बराबर ही होते हैं। लेकिन जिस भाव से, जिस तन्मयता से कोई कर्म किया जाता है वही उसे ऊँचा और नीचा बनाता है। वेदों का उच्चारण यदि मन लगाकर ध्यान से किया जाता है तो वह ऊँचा कर्म है। उसी तरह मन लगाकर ध्यान से खाना पकाया जाता है तो वह भी ऊँचा कर्म है। और भारत में तो ब्राह्मण लोग खाना बनाया ही करते थे। अब भी बनाते हैं। उनके वेदोच्चारण करने के कर्म में और खाना बनाने में बहुत अंतर है। पर वेदोच्चारण ऐसा किया जाए जैसे बेगार काटनी हो, या खाना ऐसे बनाया जाये जैसे सिर पर पड़ा कोई भार किसी तरह हटाना हो, तो दोनो की कर्म गडबड़ हो जाएंगे।
परा-अपरा और वर्ण व्यवस्था पर भी अनेक व्याख्याऐं होंगी। उन व्याख्याओं को देख-परखकर आज के संदर्भ में भारतीय मानव व काल की एक नई व्याख्या कर लेना ही विद्वता का उददेश्य हो सकता है। परंपरा का इस प्रकार नवीनीकरण करते रहना मानस को समयानुरूप व्यवहार का मार्ग दिखाते रहना ही हमेशा से ऋषियों, मुनियों और विद्वानों का काम कर रहा है।